बचाओ बाघों को: जंगल के राजा के लिए दुनिया एकजुट
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर उठी संरक्षण की पुकार, 2025 की थीम – वैज्ञानिक रणनीति और साझेदारी से होगा बाघों का भविष्य सुरक्षित

प्रकृति का गौरव, जंगल का नायक और पारिस्थितिक संतुलन का प्रहरी – बाघ आज संकट में है। हर साल 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस न सिर्फ इस शानदार जीव के अस्तित्व की याद दिलाता है, बल्कि हमें यह संकल्प लेने का अवसर भी देता है कि प्रकृति के राजा को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। 2025 की थीम बाघों के संरक्षण के लिए विज्ञान-आधारित रणनीति और वैश्विक सहयोग पर जोर देती है।
भिलाई। हर साल 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस न केवल इन शक्तिशाली प्रजातियों की गरिमा का उत्सव है, बल्कि यह उनके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की याद भी दिलाता है। बाघ, जो अपनी नारंगी-काली धारियों, पैनी आँखों और मांसल शरीर से जंगल की शोभा बढ़ाते हैं, अब विलुप्ति के कगार पर हैं।

बाघों की छह प्रमुख उप-प्रजातियाँ हैं — बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, सुमात्रन टाइगर, इंडोचाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर और दक्षिणी चीनी टाइगर। इनमें बंगाल टाइगर भारत की शान है, जो दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत बाघों का घर है।
बाघ केवल शिकारी नहीं हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति जंगल के स्वास्थ्य और जैव विविधता का संकेत होती है।
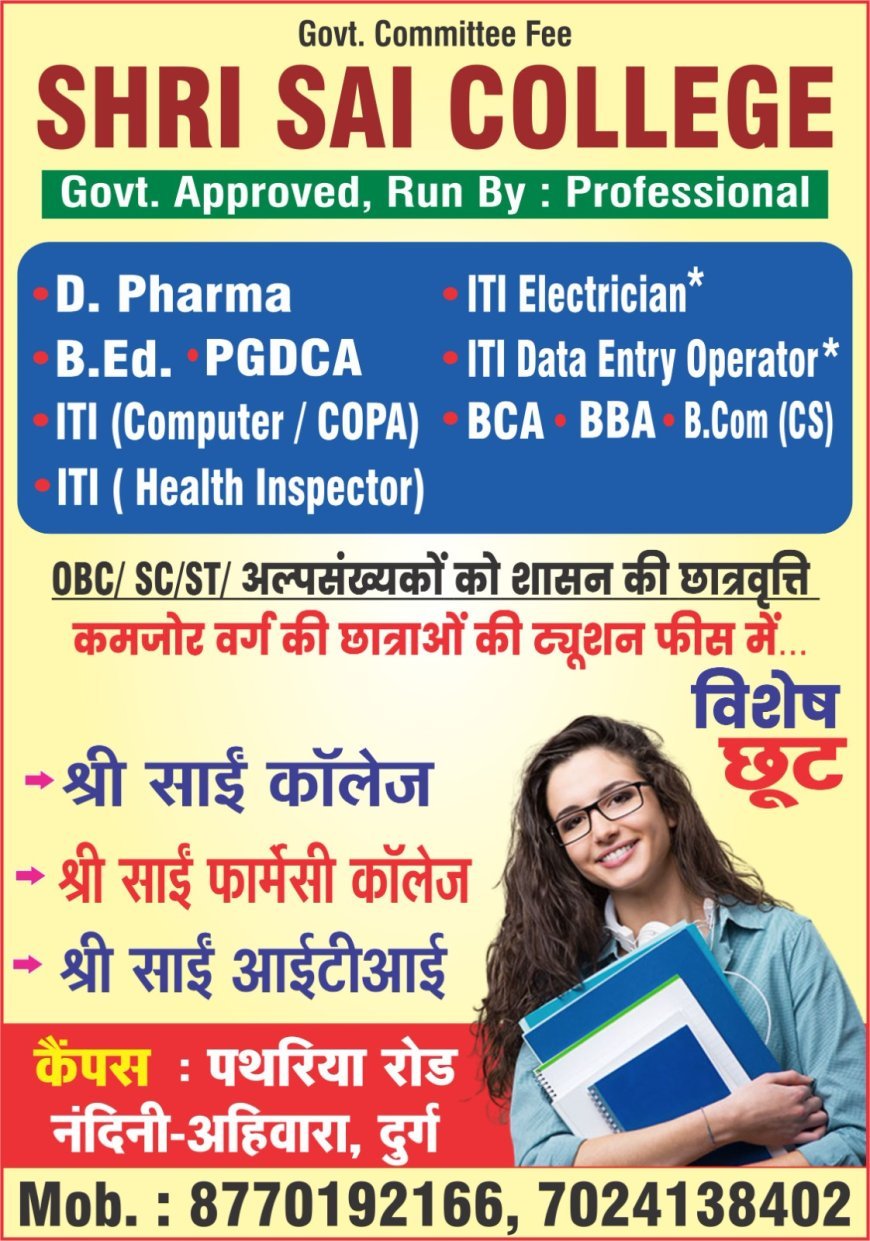
2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट के दौरान, जब सामने आया कि बीसवीं सदी में 97% बाघ विलुप्त हो चुके हैं, तब बाघ रेंज वाले 13 देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था — जनजागरूकता बढ़ाना, शिकार और वन विनाश के खिलाफ आवाज उठाना, और संरक्षण की ठोस रणनीति बनाना।

इस वर्ष की थीम है — “बाघ संरक्षण: विज्ञान आधारित और सहयोगात्मक रणनीति”
यह थीम बाघ रेंज वाले देशों को साझा प्रयास, वैज्ञानिक हस्तक्षेप, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और तकनीकी नवाचारों के ज़रिये संरक्षण को प्रभावी बनाने का संदेश देती है।
पर्यावरण प्रेमी प्रशांत कुमार क्षीरसागर ने इस अवसर पर कहा, “29 जुलाई केवल तारीख नहीं, बल्कि यह प्रकृति और भविष्य के बीच एक सेतु है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन अनमोल जीवों को बचाने में अपना योगदान दे।” बाघों के लिए सुरक्षित आवास, अवैध शिकार पर सख्ती, जनसंख्या की मॉनिटरिंग, और स्थानीय समुदायों की सहभागिता को इस अभियान का आधार बनाया गया है।






 suntimes
suntimes 